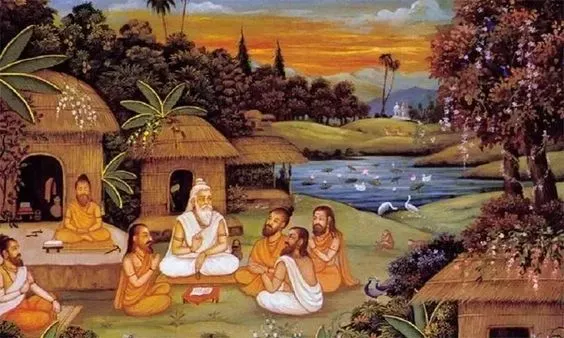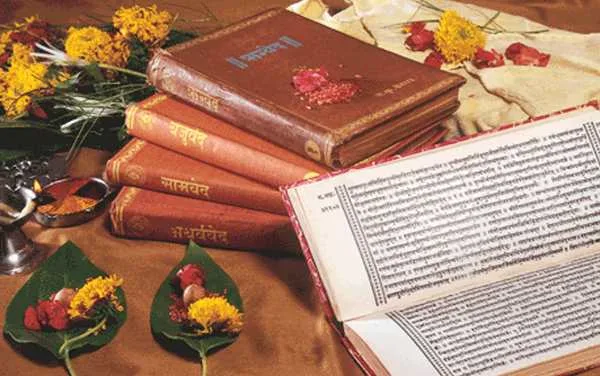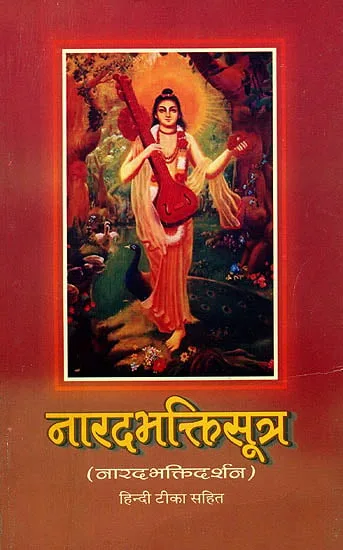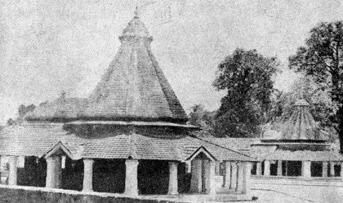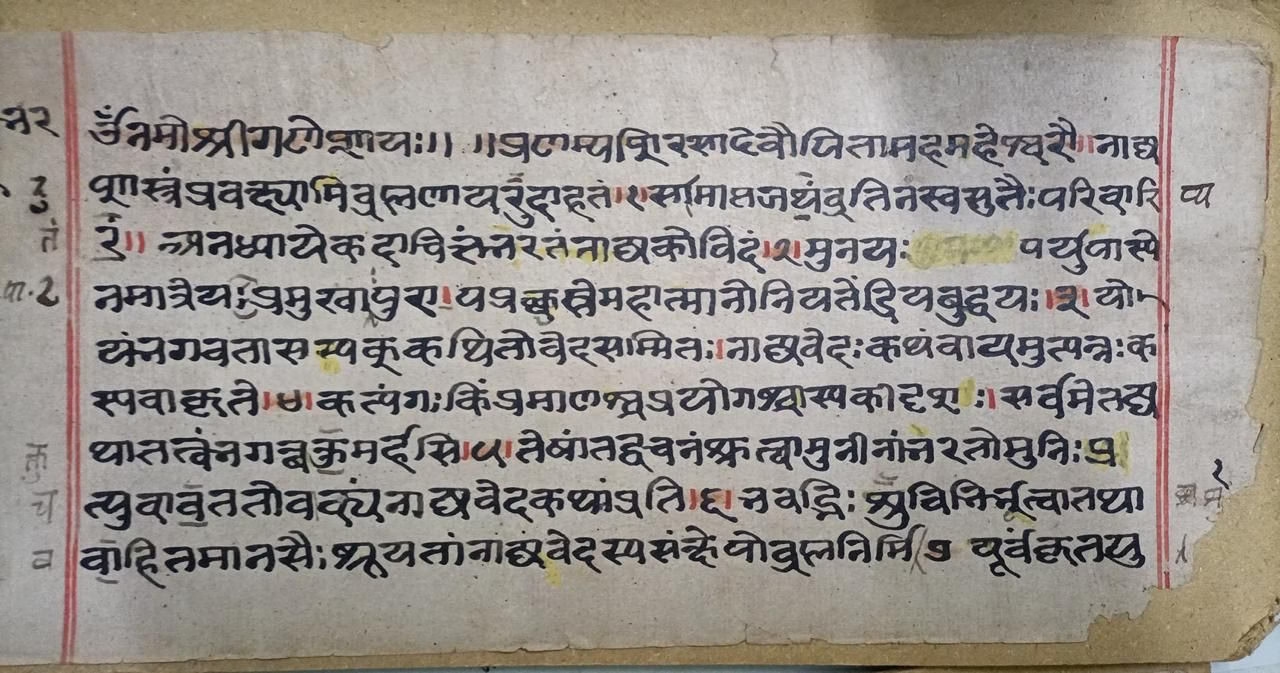भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर अनेक महान व्यक्तित्वों से समृद्ध रही है। इनमें से दो ऐसे स्तंभ हैं, हनुमान जी, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वीरगाथा आधुनिक भारतीय इतिहास में अमर है। इन दोनों महापुरुषों के जीवन, आचरण और आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
हनुमान जी: सेवा, शक्ति और समर्पण का प्रतीक
हनुमान जी को केवल बलशाली देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आदर्श सेवक, निष्ठावान भक्त और बुद्धिमान नायक के रूप में भी जाना जाता है। उनका सम्पूर्ण जीवन श्रीराम के प्रति पूर्ण समर्पण, धर्म के प्रति निष्ठा, और संकट के समय अडिग साहस का प्रतीक है।
निःस्वार्थ सेवा: उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन यह सिखाता है कि सेवा तभी पवित्र होती है जब उसमें स्वार्थ न हो।
बुद्धि और बल का संतुलन: ‘बुद्धिमत्ता’ और ‘शौर्य’ का ऐसा संतुलन विरले ही देखने को मिलता है।
धर्म रक्षक: जब रावण जैसे अत्याचारी सामने हों, तो धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही सच्चा कर्म है।
हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल साधु भाव से नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर साहस और सामर्थ्य से भी करनी होती है।
शिवाजी महाराज: आत्मसम्मान, शासन और सांस्कृतिक अस्मिता के नायक
शिवाजी महाराज का जीवन ऐसे समय में शुरू हुआ जब भारतवर्ष पर विदेशी शासन का अंधकार छाया हुआ था। उन्होंने केवल एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि भारतीय संस्कृति, मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए आत्मबलिदान और रणनीति का अद्भुत परिचय दिया।
स्वराज्य की स्थापना: उनका सपना केवल एक भूभाग जीतने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने का था जहां लोगों को सम्मान और आत्मगौरव मिले।
गौरवशाली परंपराओं की रक्षा: जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब जनमानस का आत्मविश्वास डगमगा रहा था, तब शिवाजी महाराज एक ऐसे दीपक बने जिन्होंने हिन्दवी स्वराज्य का प्रकाश फैलाया।
न्यायप्रिय और धार्मिक सहिष्णु: वे अपने शासन में सभी धर्मों को सम्मान देते थे, परंतु अपनी सांस्कृतिक जड़ों से डिगे नहीं। यही संतुलन आज के भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उनका चरित्र आज के युवाओं के लिए यह संदेश देता है कि बिना अपनी अस्मिता खोए, हम आधुनिक भी बन सकते हैं, और न्यायप्रिय भी।
दो युगों, एक संदेश: धर्म और राष्ट्र की रक्षा
हनुमान जी ने त्रेतायुग में श्रीराम की सेवा कर धर्म की रक्षा की, तो शिवाजी महाराज ने कलियुग के अंधकार में प्रकाश बनकर संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा की।
दोनों ही चरित्र यह दर्शाते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है, तब एक समर्पित और साहसी नायक खड़ा होता है: चाहे वह वानर शरीरधारी हनुमान हो या सिंहगर्जना करता मराठा वीर।
आज भारत को ऐसे ही चरित्रों की आवश्यकता है: जो सेवा में नतमस्तक हों, लेकिन जब जरूरत पड़े तो धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए अडिग खड़े हों।
हनुमान जी और शिवाजी महाराज दो युगों के दो आदर्श हैं, एक दैवीय, दूसरा मानव रूप में। दोनों का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन है; और राष्ट्रप्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि साहस, त्याग और विवेक का समुच्चय है।
यदि आज का युवा इन दोनों पथप्रदर्शकों से शिक्षा ले, तो वह न केवल एक सशक्त नागरिक बन सकता है, बल्कि भारत को एक बार फिर आत्मगौरव और सांस्कृतिक स्वाभिमान के शिखर पर पहुंचा सकता है।